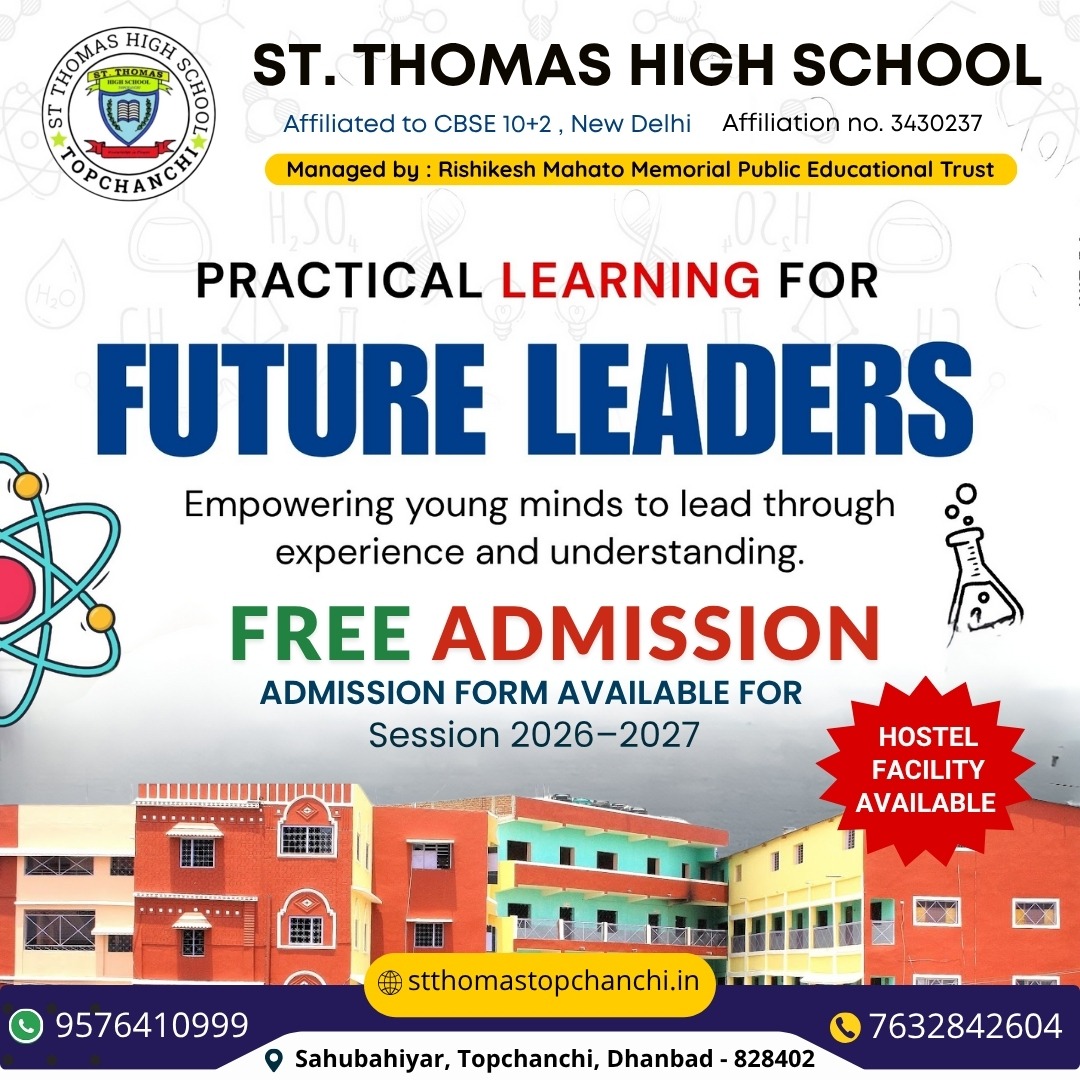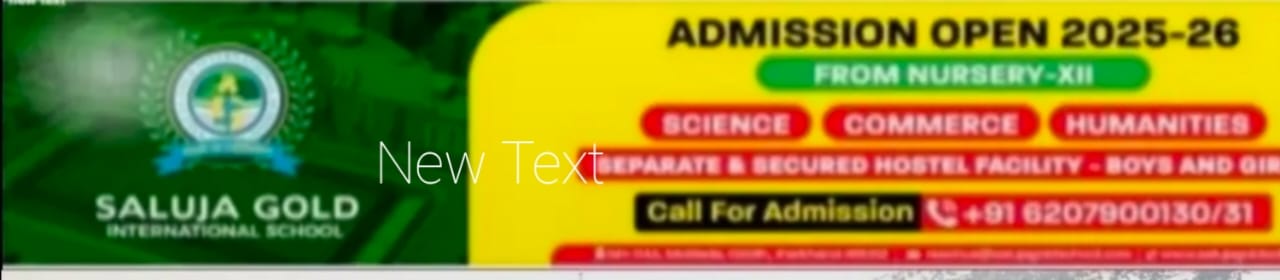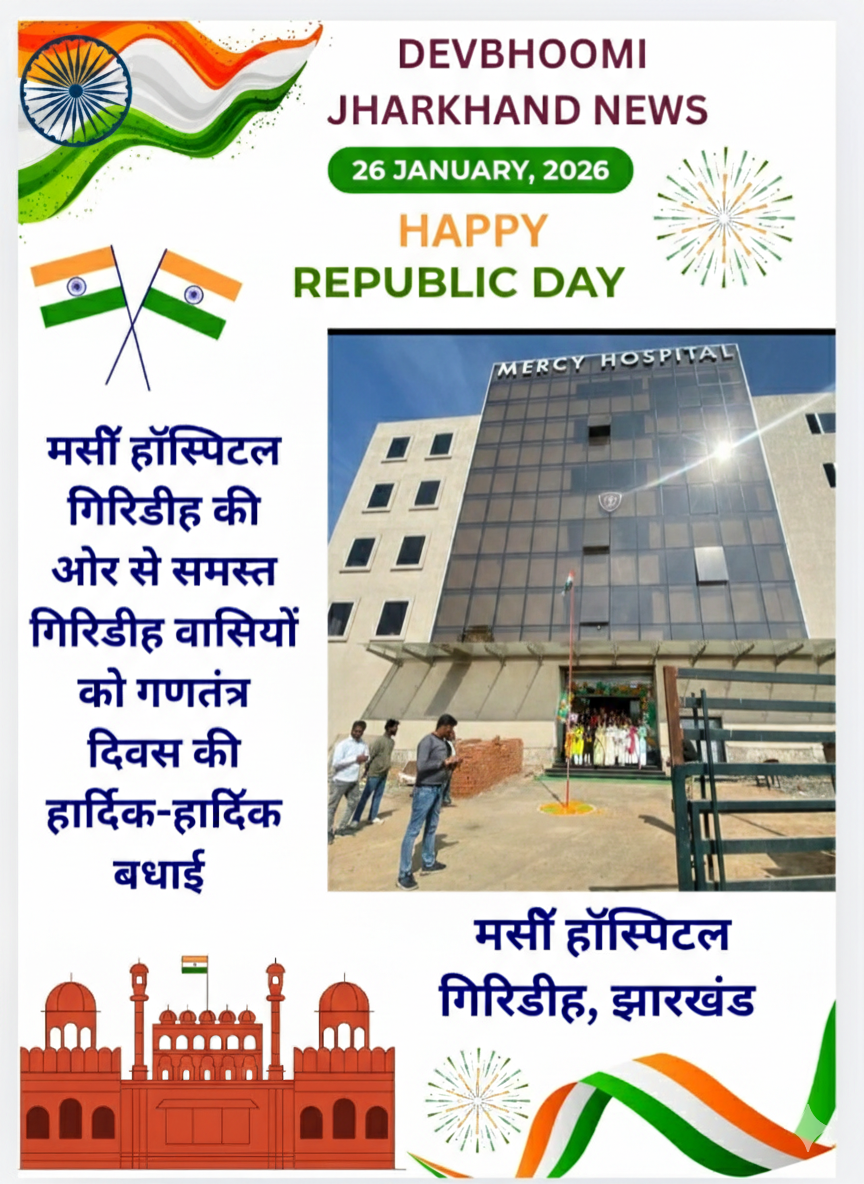
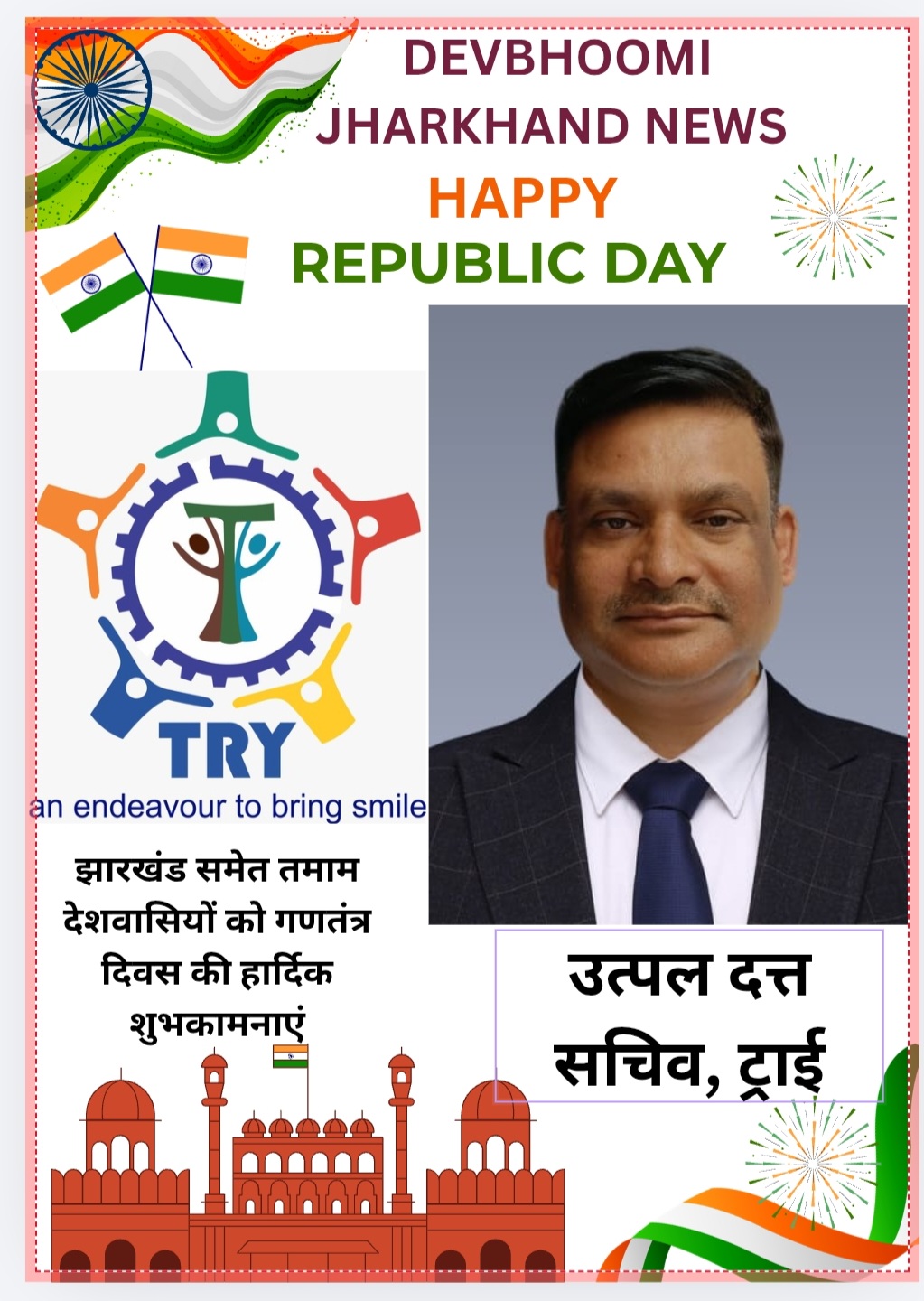



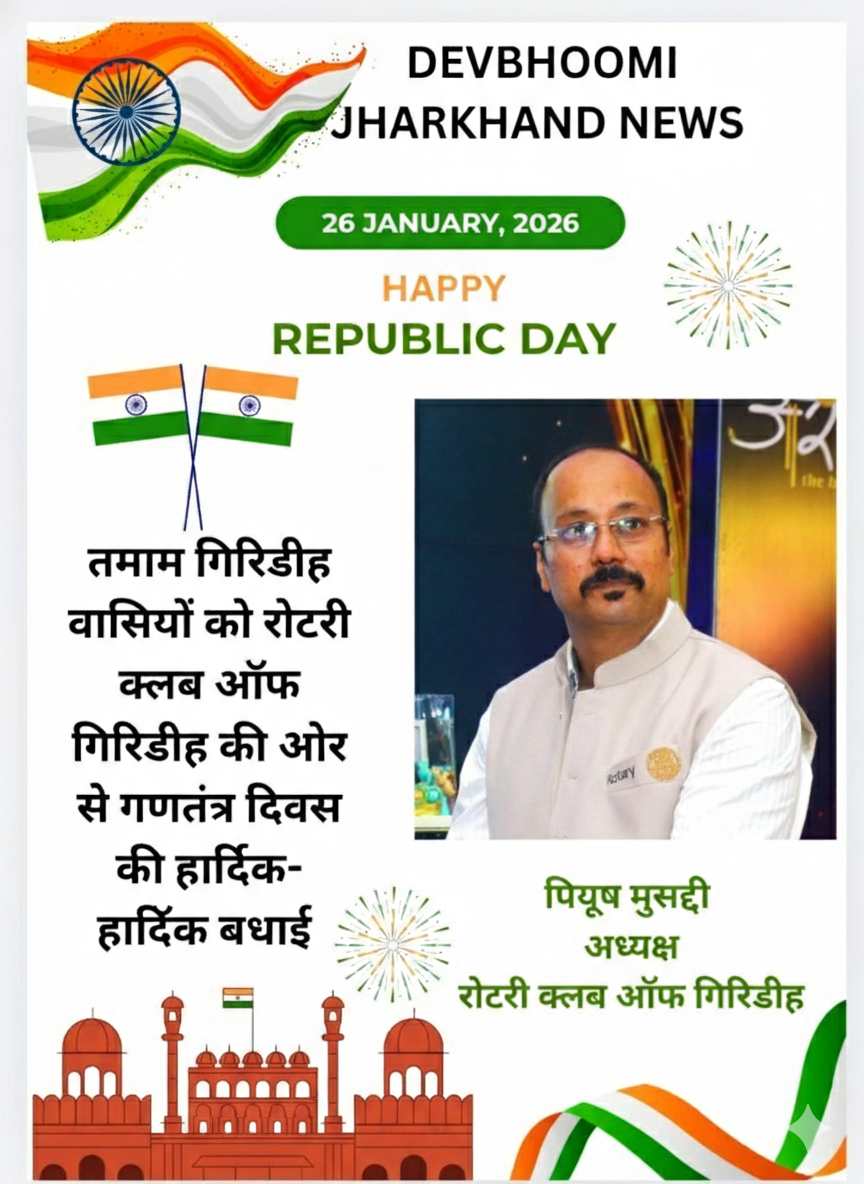


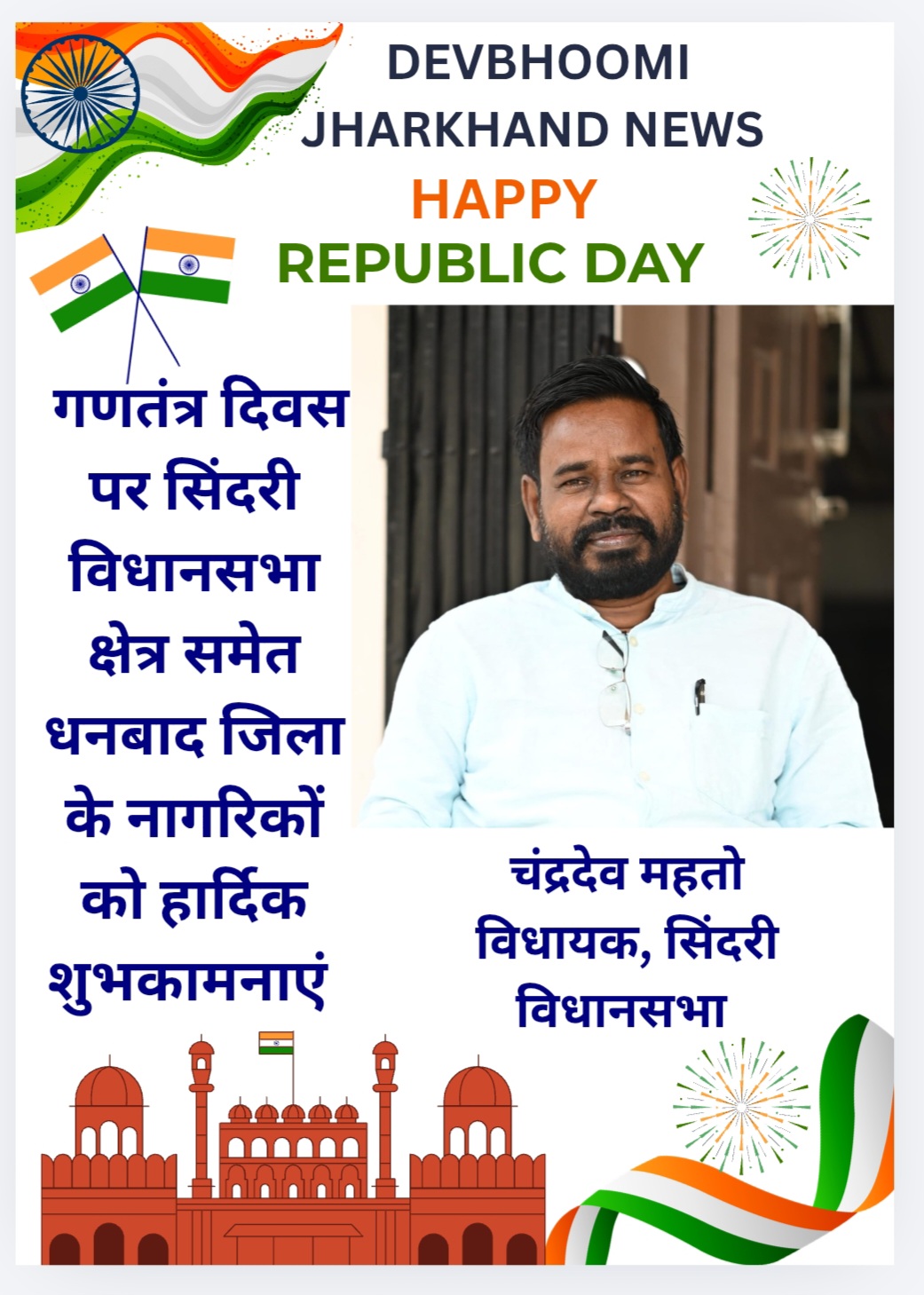
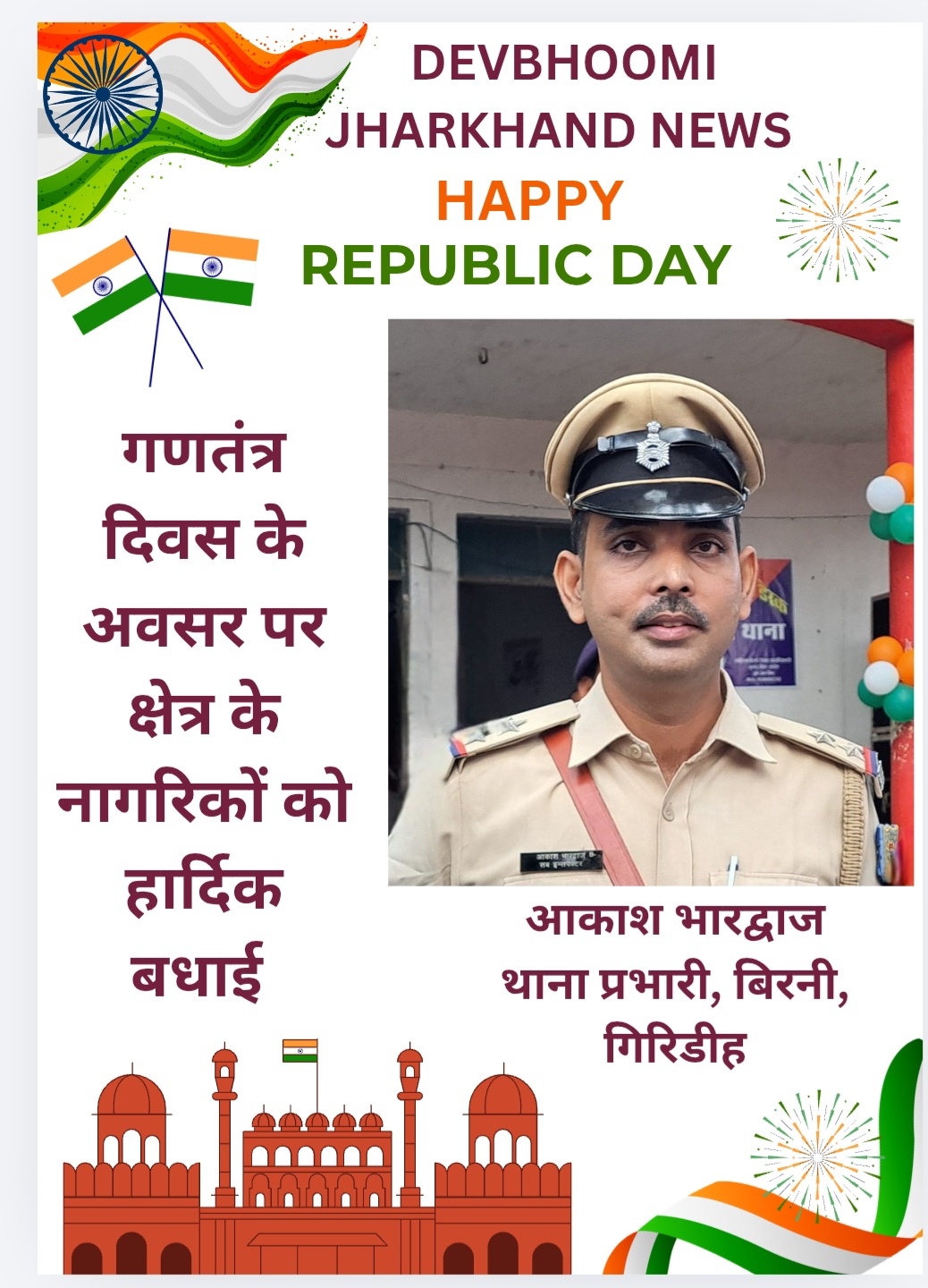

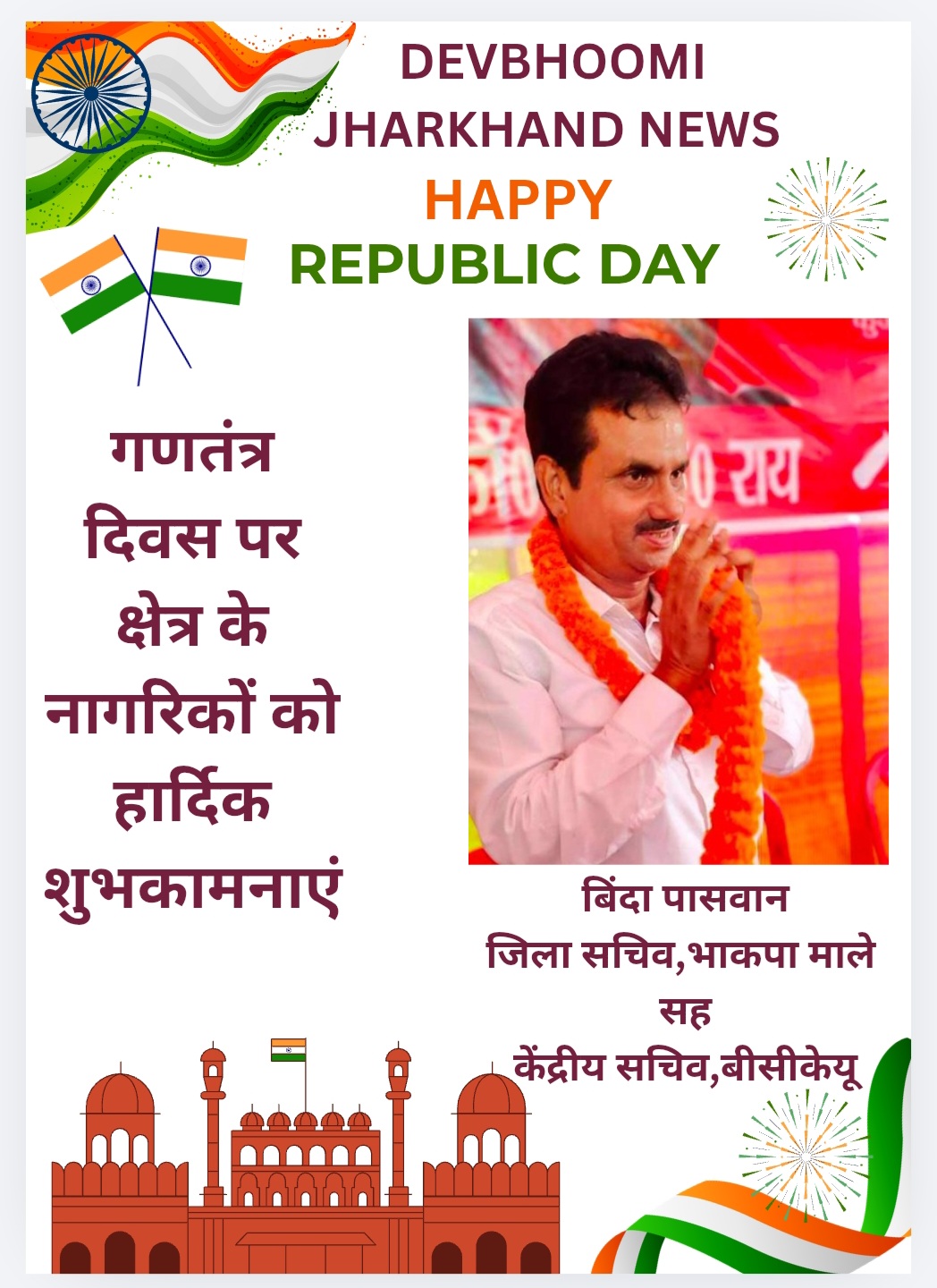



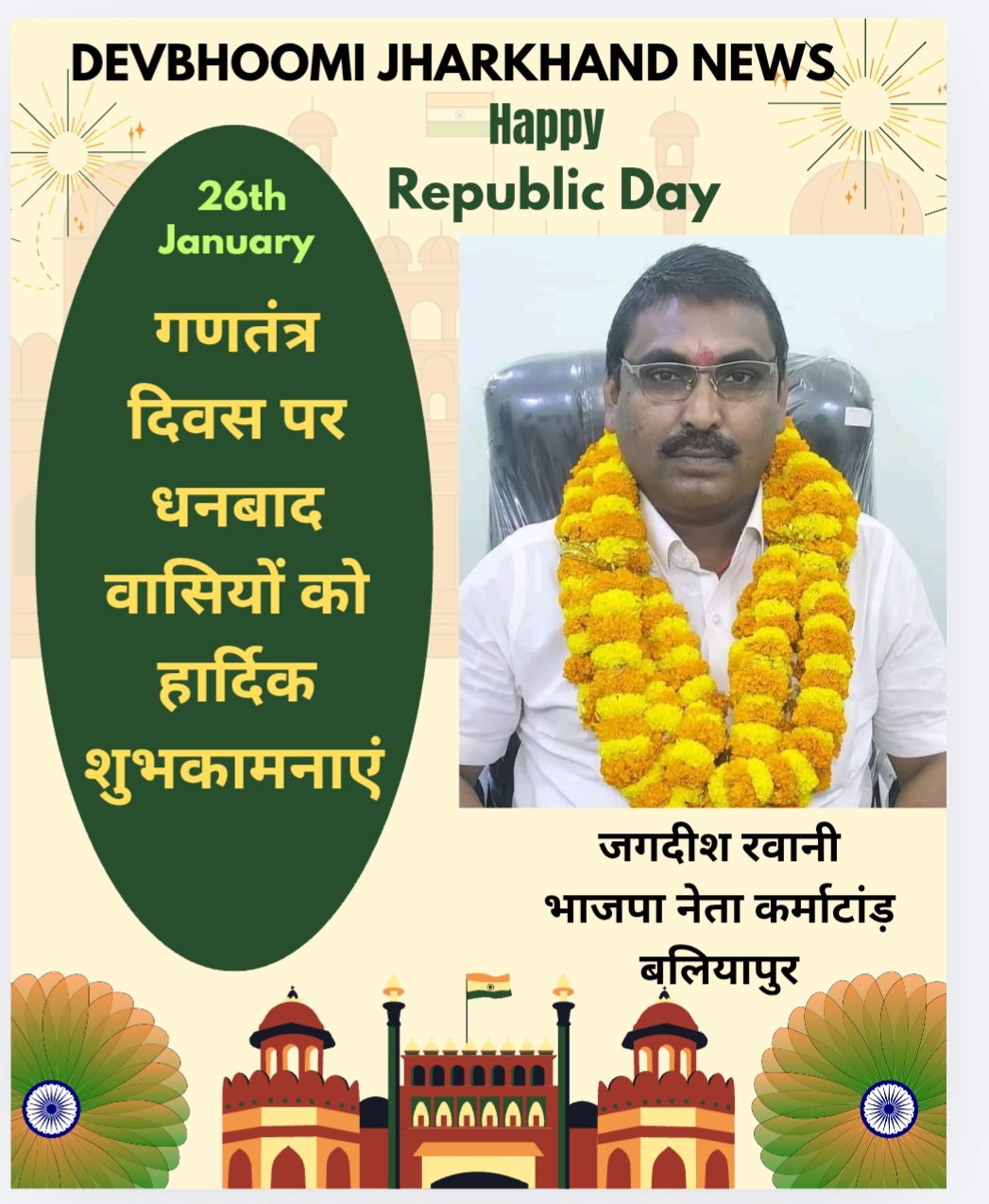



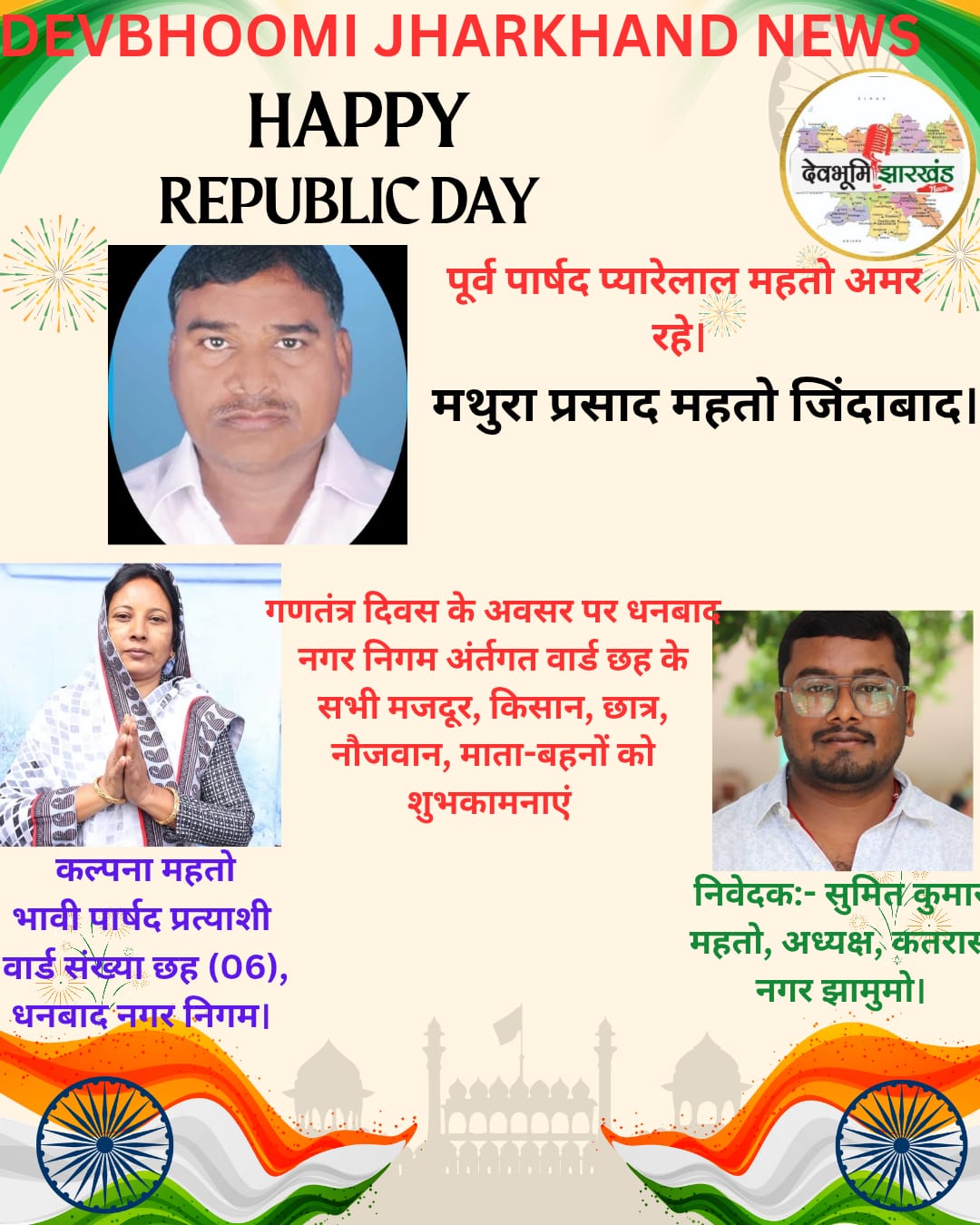





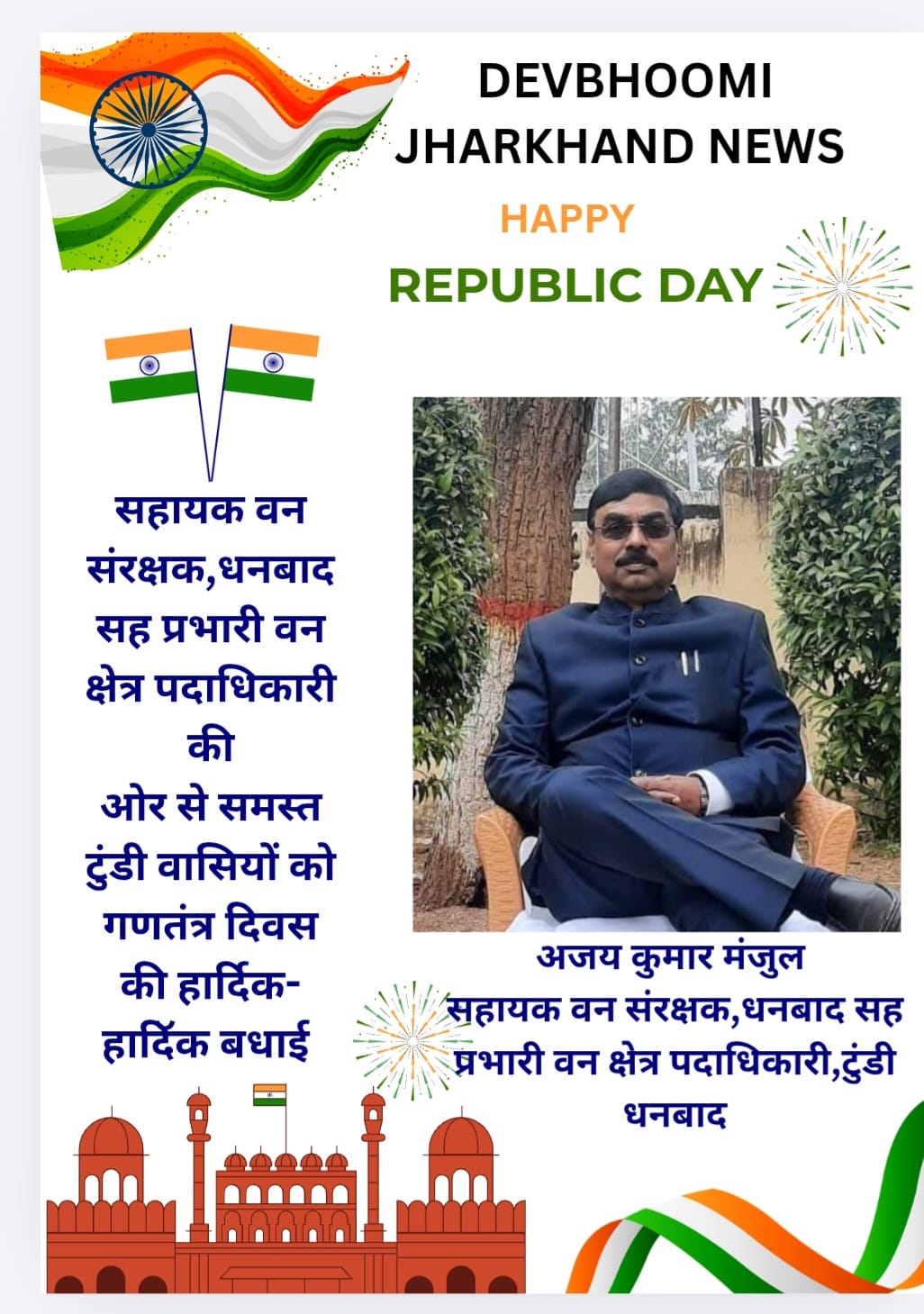



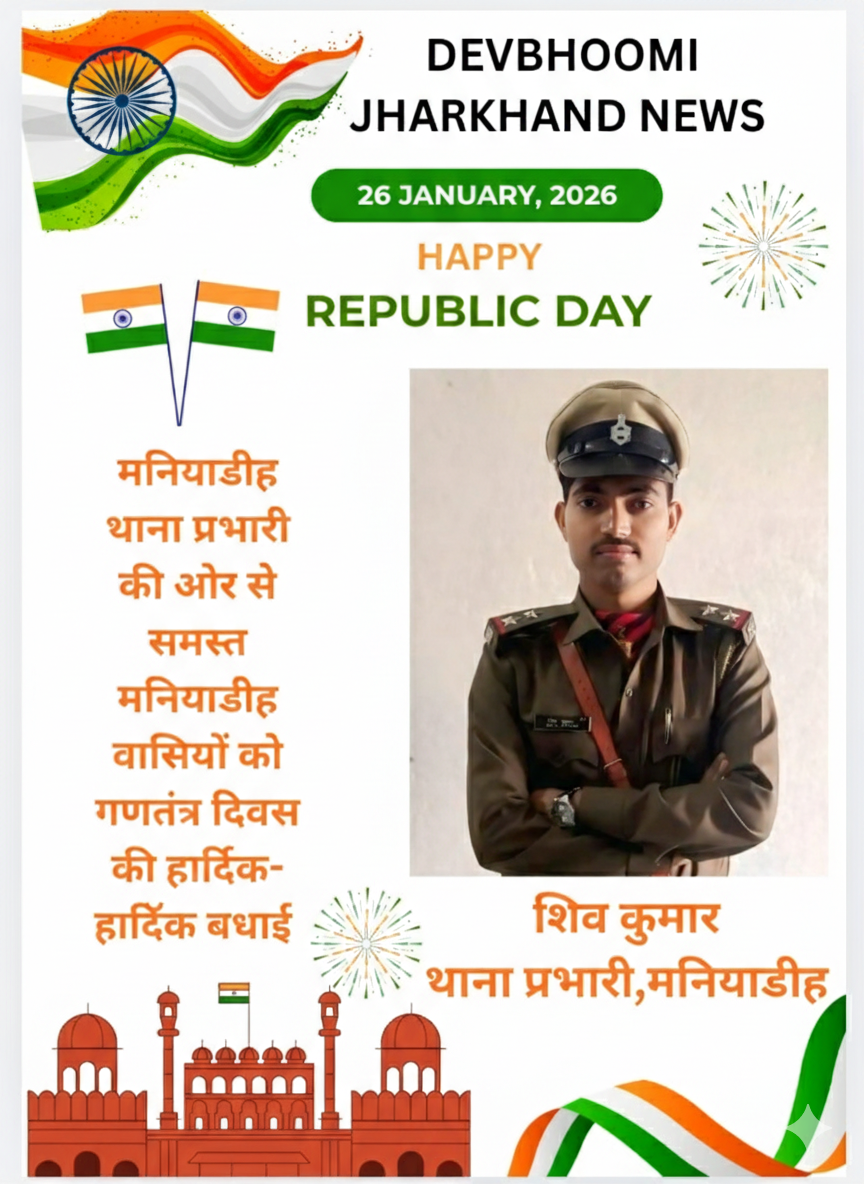
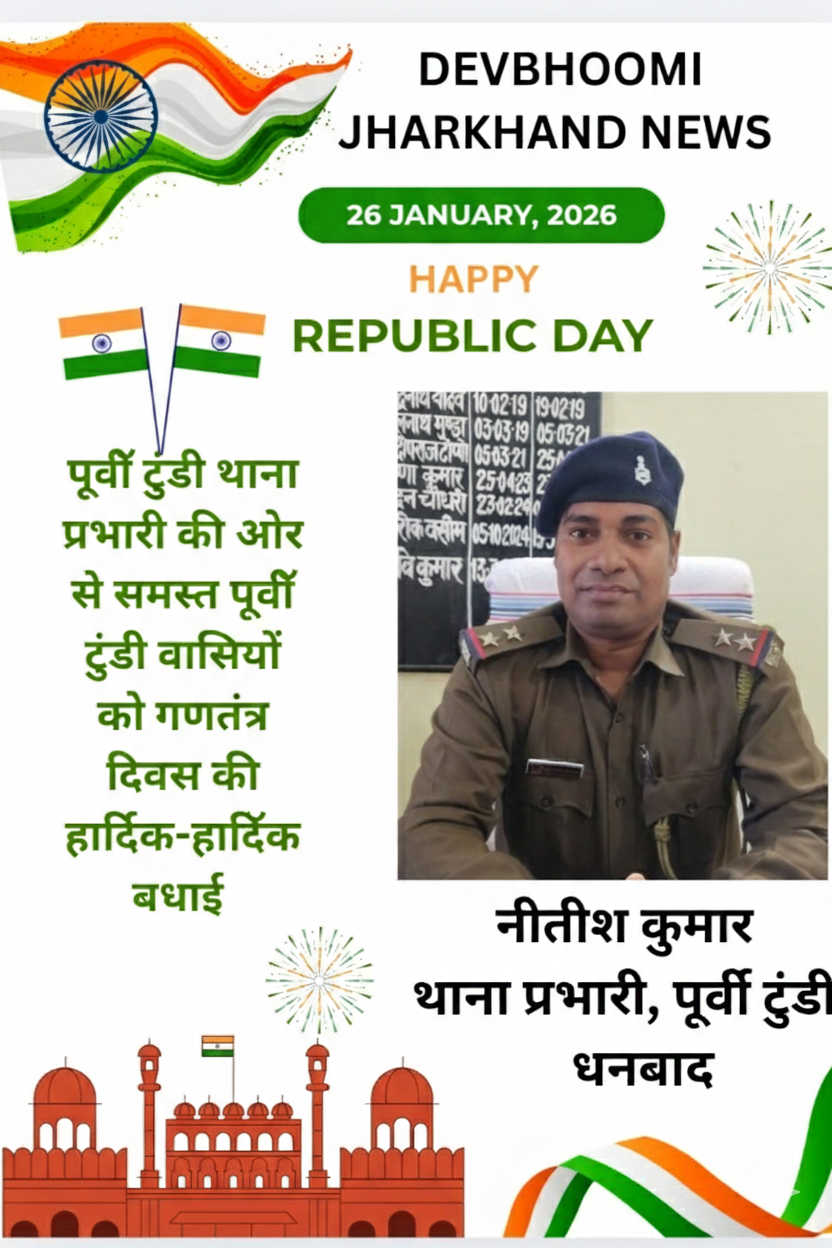

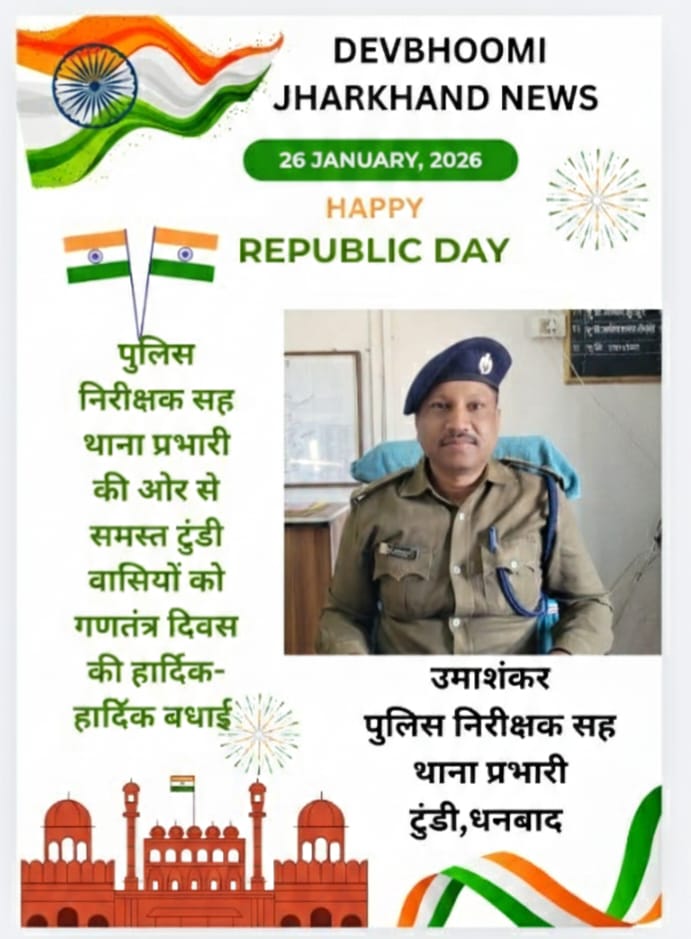
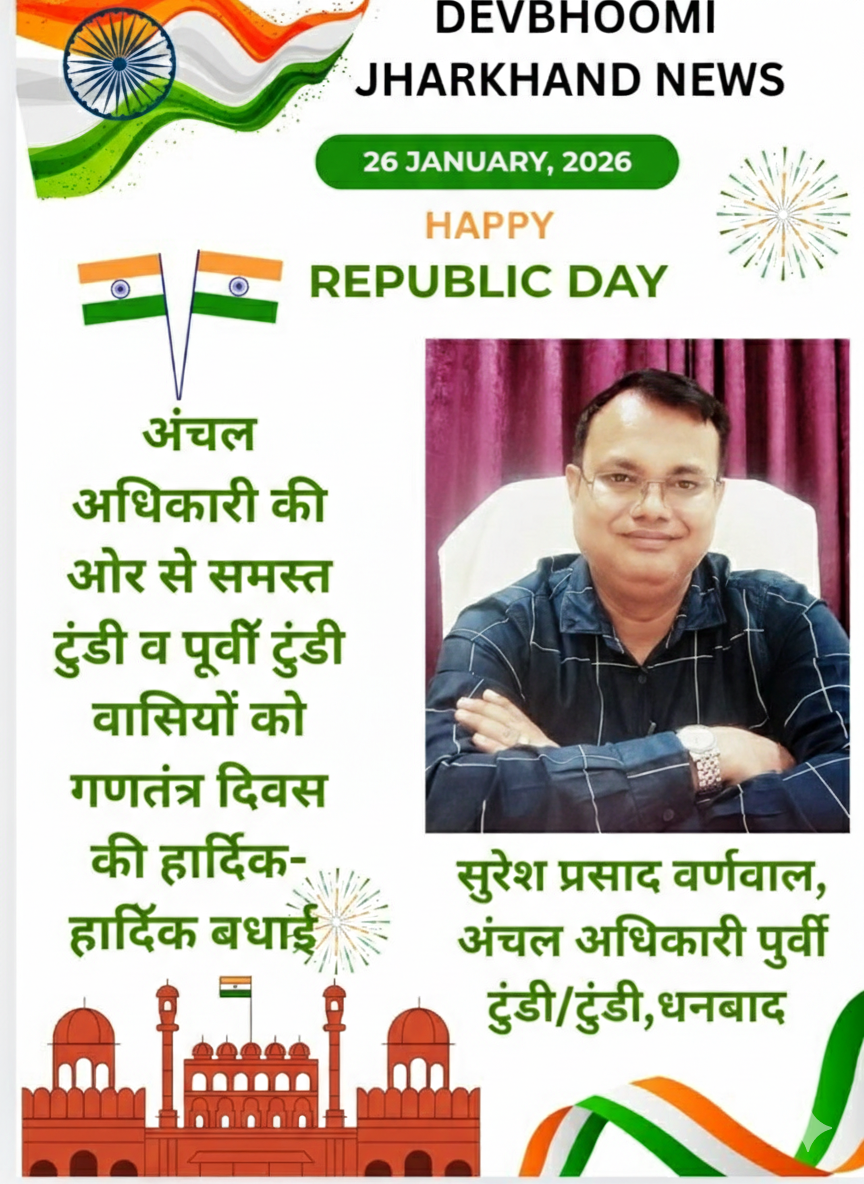
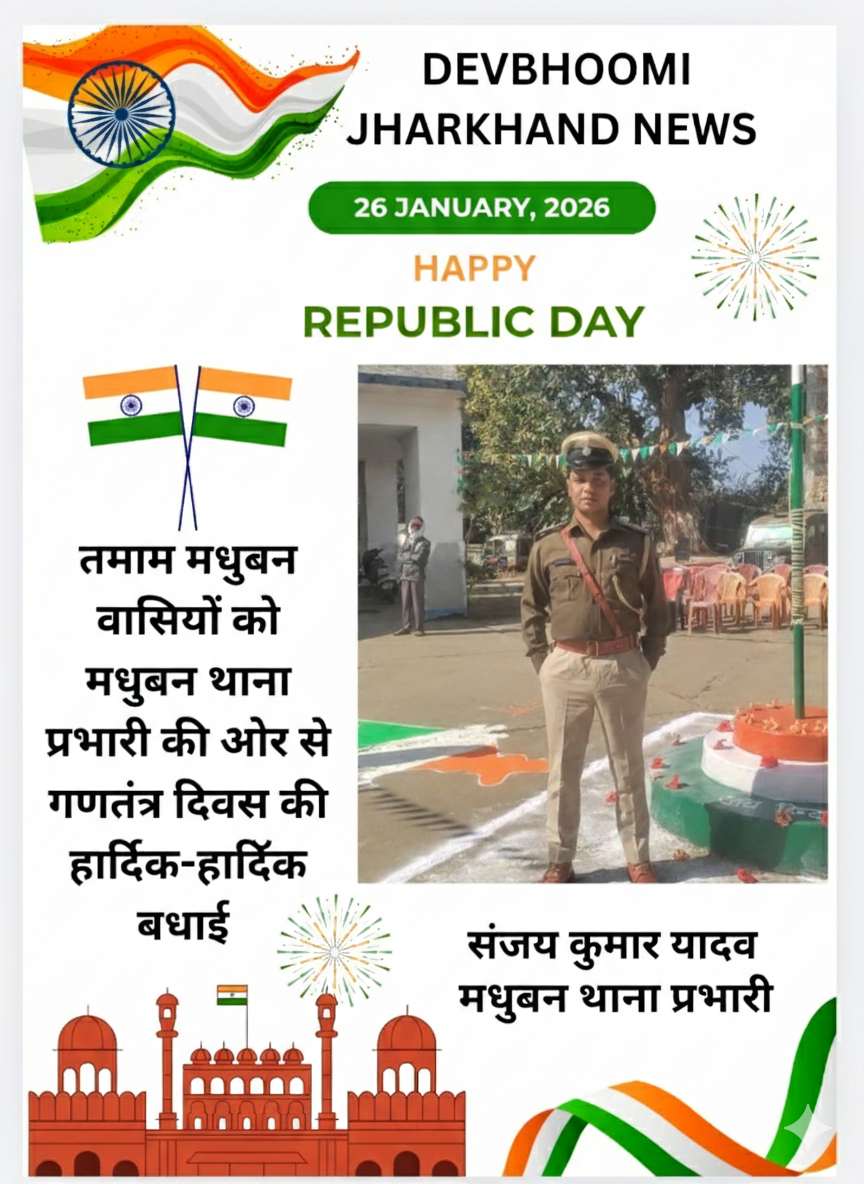
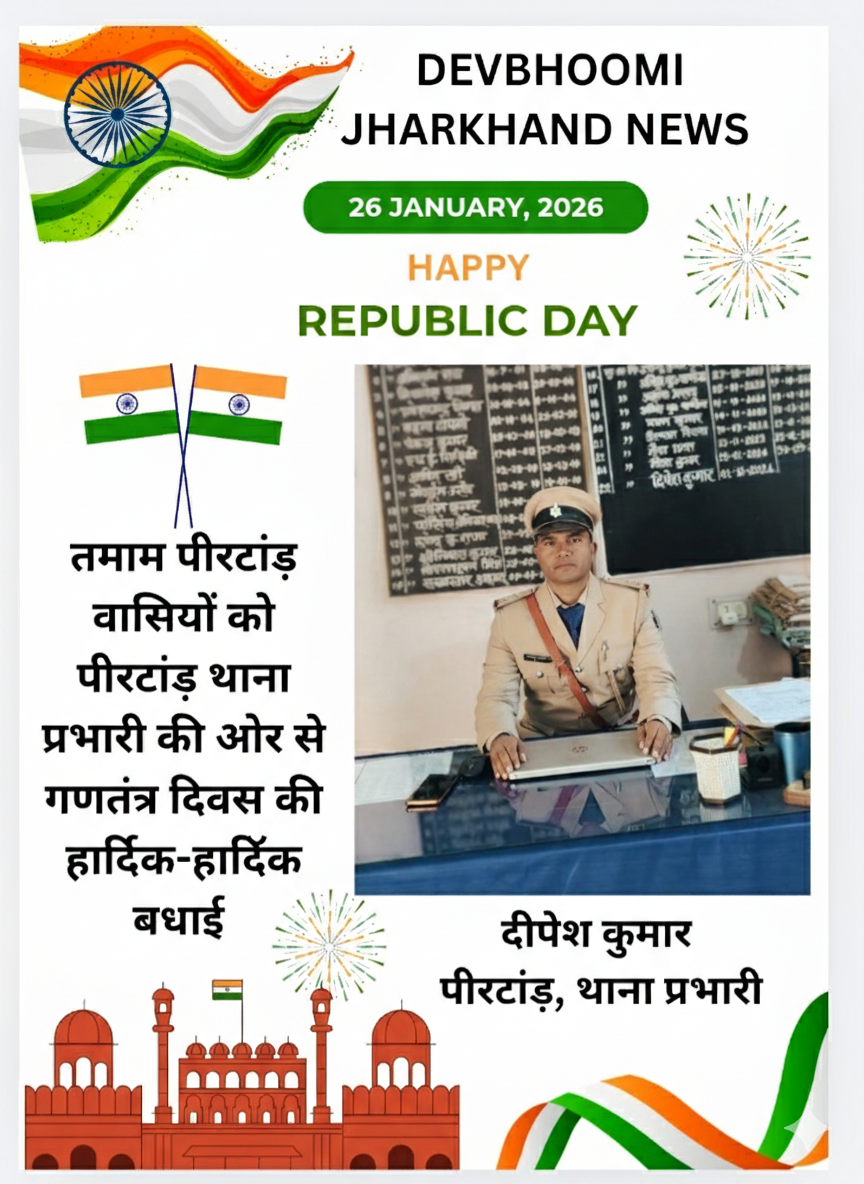
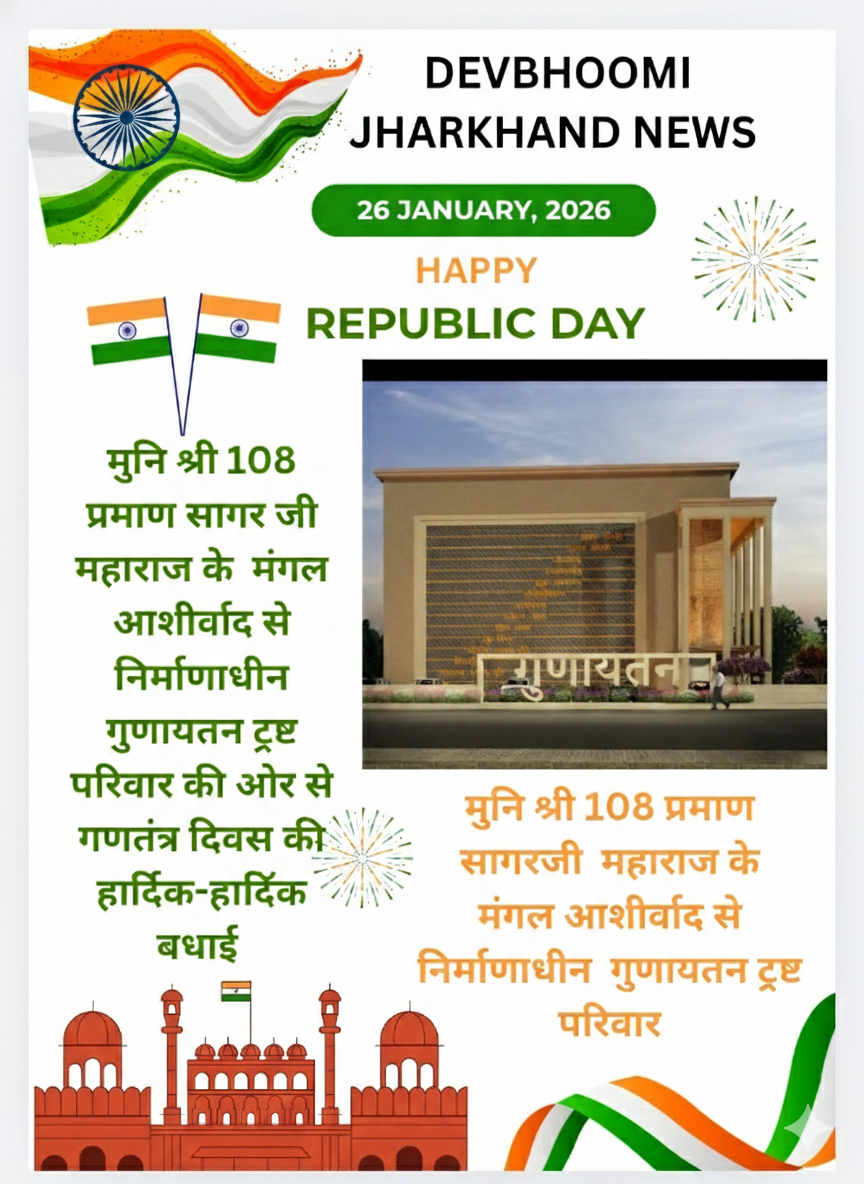


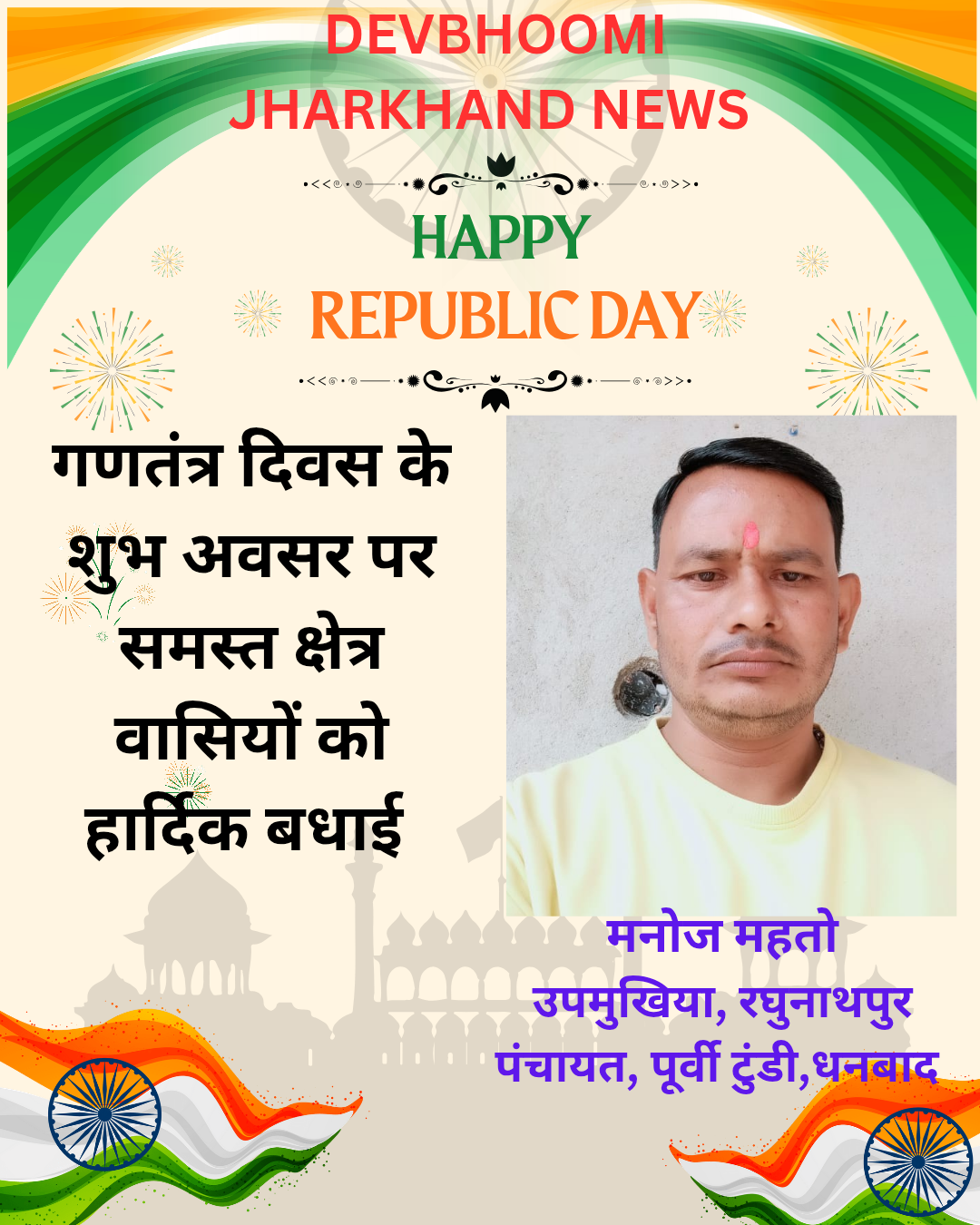




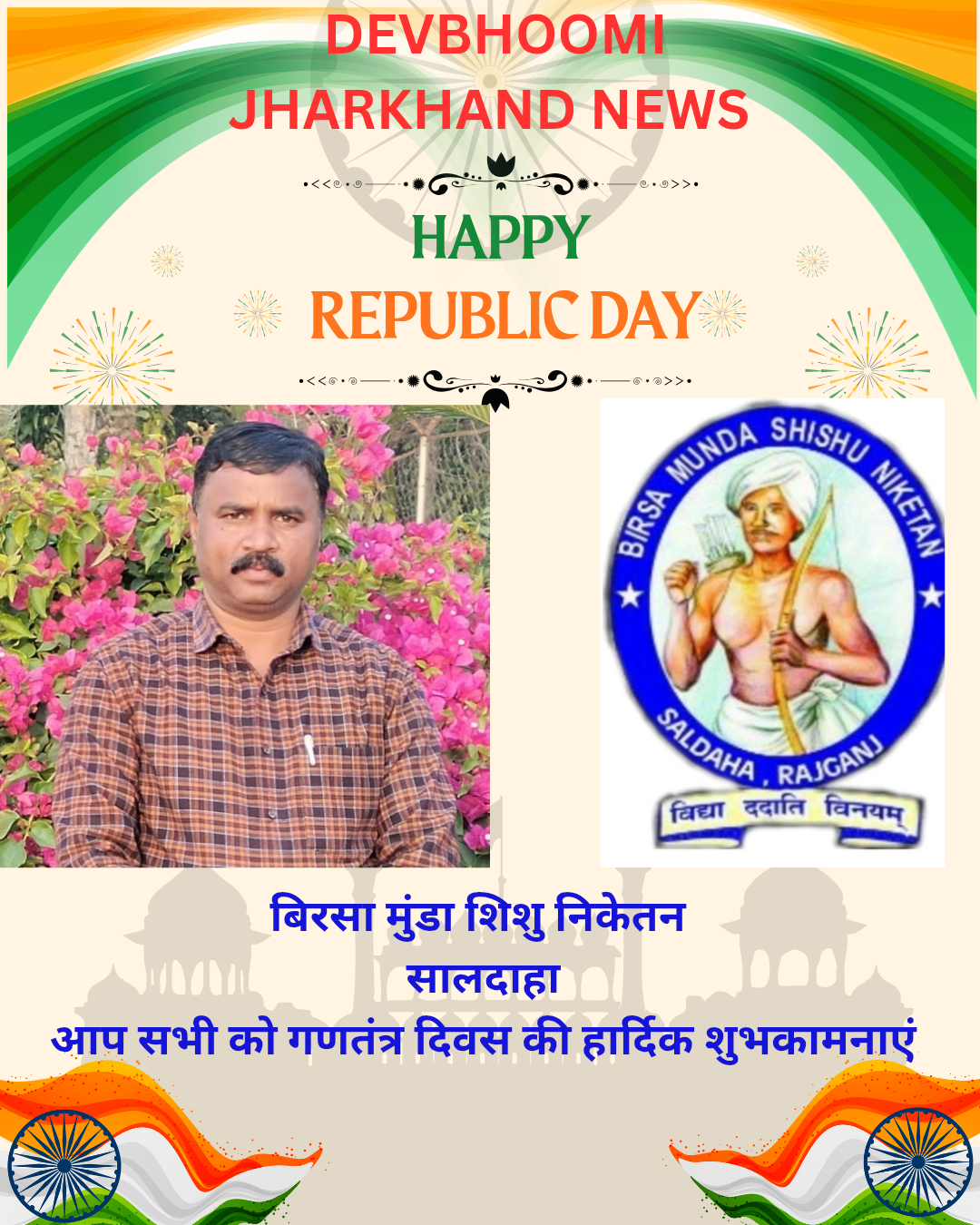

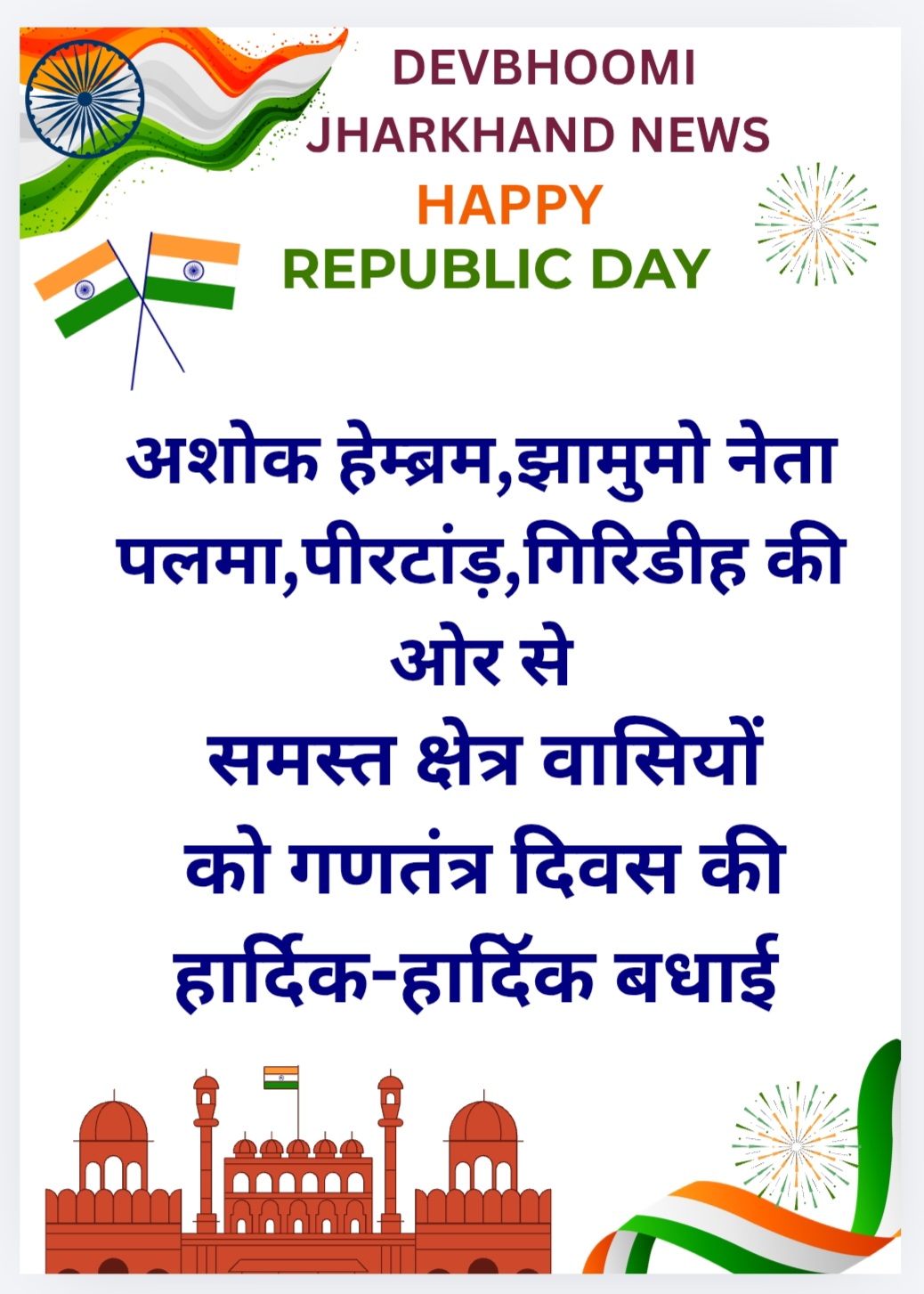
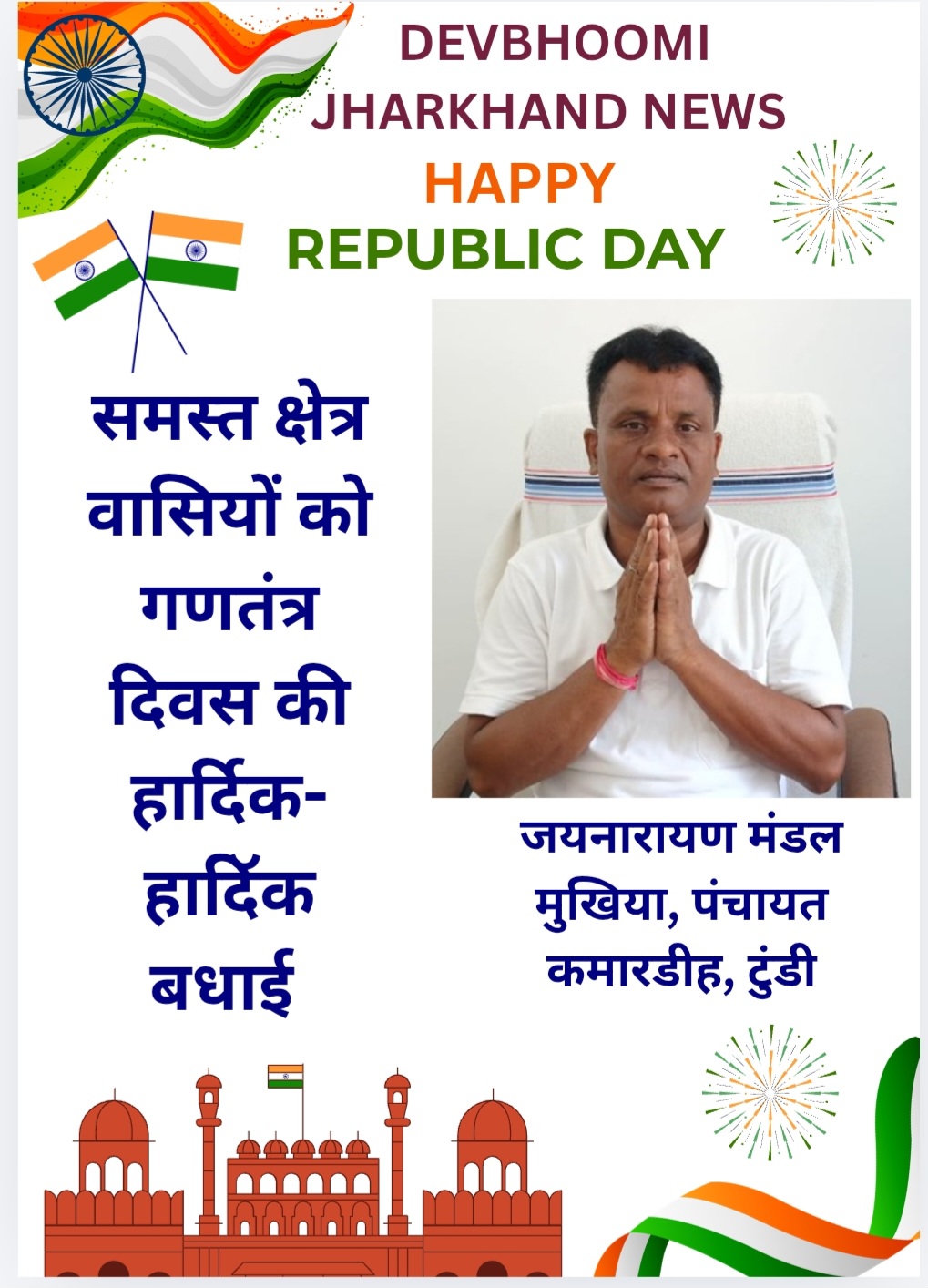

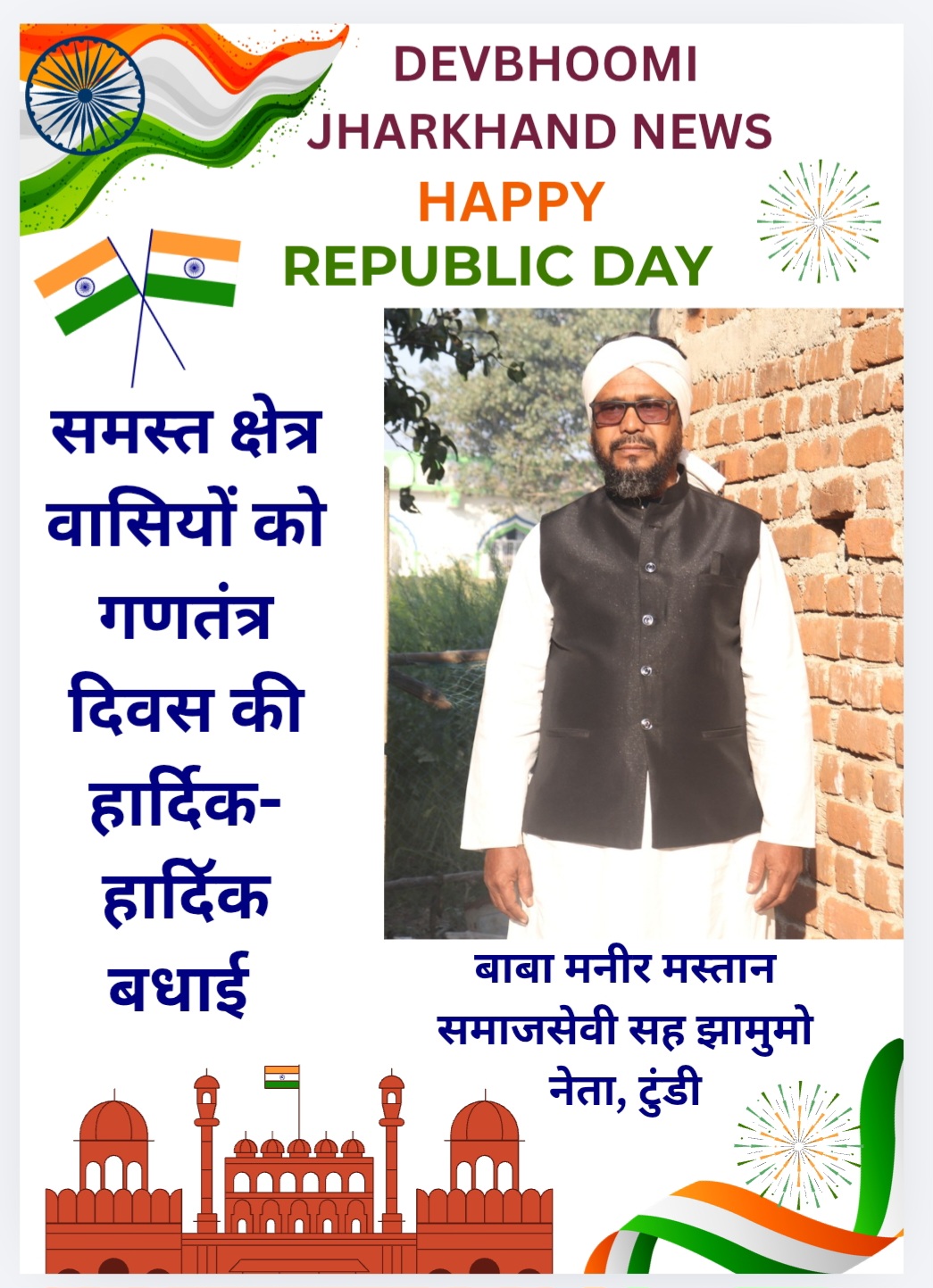
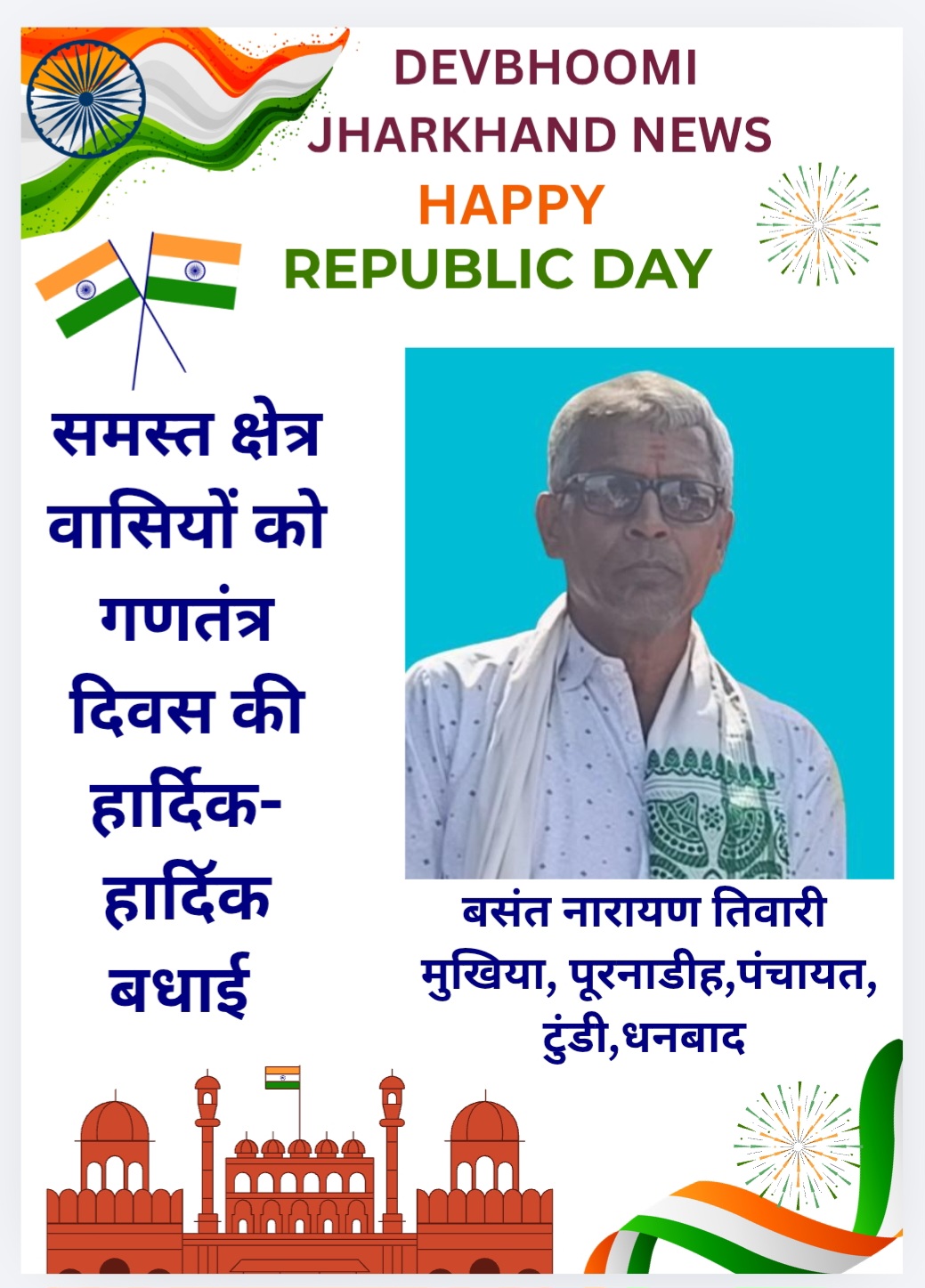
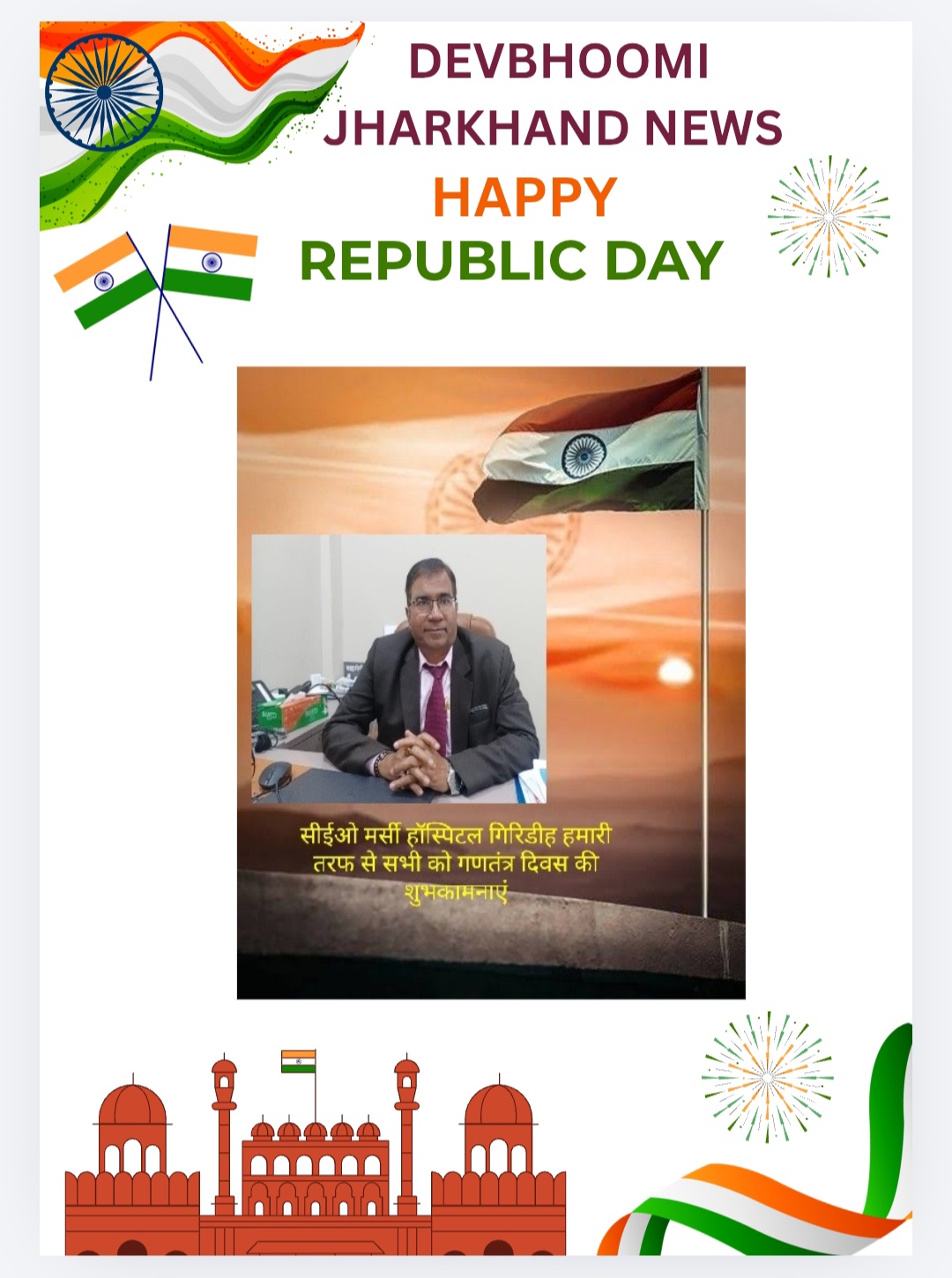
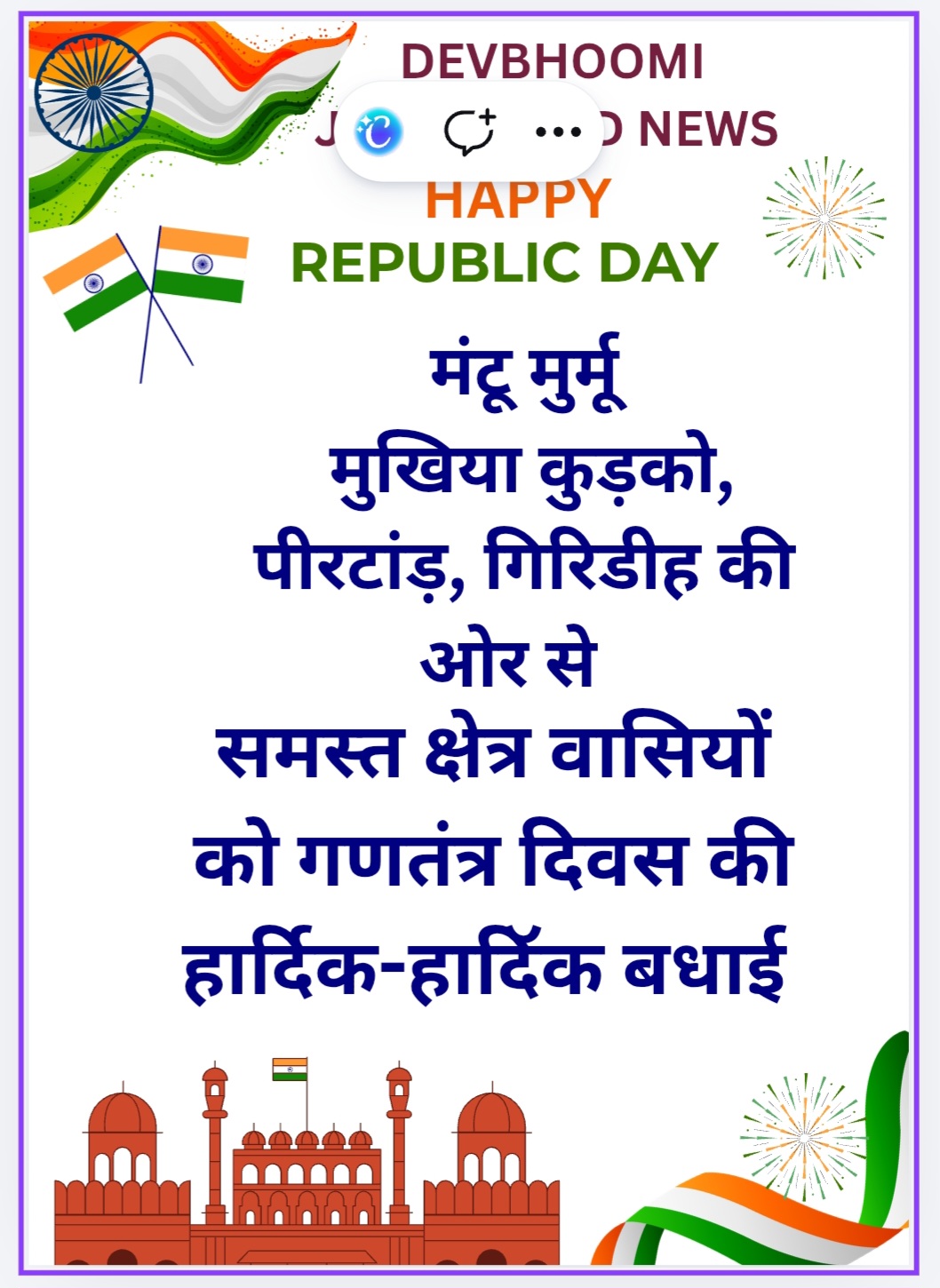

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्वयं खड़ी हिन्दी और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेंगे तो बच्चे स्वतः अनुकरण करेंगे

हिन्दी दिवस पर एक शिक्षक की कलम से
दुनिया की कोई भी भाषा सीधे अवतरित नहीं हुई है। सारी भाषाओं का उद्विकास ही हुआ है। मेरी दृष्टि में यह विकास क्रम संकेत, ध्वनि, बोली, लिपि होते हुए लिखित में परिणत हुआ होगा। मानव सभ्यता का विकास भाषा के बिना असंभव था क्योंकि भाषा ही परस्पर संवाद का माध्यम होती है। यही सभ्यता और संस्कृति का आधार होती है। भाषा इतिहास की साक्षी होती है। अतः भाषा का विकास क्रम सामाजिक और बौद्धिक विकास को जानने और समझने का बेहतर माध्यम हो सकता है। वैसे भी भाषा को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सहयात्री माना जाता है। भाषा के रूप में हिन्दी का विकास भी क्रमिक रूप में हुआ। हिंदी का विकास विभिन्न मिश्रित बोलियों और उपभाषाओं की समेकित व विकसित व्युत्पत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार भारत के प्रत्येक कोस में पानी और चार कोस में वाणी या बोली बदल जाती है। जैसा कि आपको पता है हिंदी करीब- करीब संपूर्ण उत्तर भारत की एक सर्वमान्य भाषा है। इस हिंदी पट्टी में हिंदी का विकास स्थानीय बोलियों की मानकीकृत या परिमार्जित द्वितीयक स्वरूप में हुआ। हिंदी का विकास इन्ही बोलियों से हुआ जिसे बाद के भाषाविदों ने देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध कर लिखित, विकसित और परिमार्जित किया। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिन्दी की कई बोलियाँ और उपभाषाएँ हैं, जैसे- शौरसेनी, बुंदेली, अवधि, दक्खिनी, मागधी, अर्द्धमागधी आदि। इन भाषाओं का विकास हिंदी से पहले ही हो चुका था। जब विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आयीं तो सबसे अधिक प्रभाव स्थानीय भाषा और संस्कृति पर पड़े। परिणामस्वरूप भाषा की मौलिकता प्रभावित हुई। स्थानीय भाषा कई आगत भाषा व बोलियों से कई शब्द अपनाने के लिए प्रेरित हुई। इसके साथ कई संश्लिष्ट संस्कार-व्यवहार तथा विकृति- स्वीकृति भी आरोपित हुए। इन बोलियों की मौलिकता अवश्य प्रभावित हुई किंतु इनका अस्तित्व बहुत हद तक सुरक्षित रहा। वहीं कुछ बोलियों में तरलता और विनिमयशीलता का अभाव दिखा। इनकी सिमटती परिधि ने कालक्रम में स्वयं को विलोपित करने को मजबूर किया या यों कहें कि ये आगत भाषा के प्रवाह को झेल नहीं पायीं। सही मायने में देखें तो इन्ही समृद्ध बोलियों ने हिन्दी के विकास में अपनी रक्त- मज्जा का दान दिया जिससे हिन्दी पल्लवित- विकसित हुई।
संपूर्ण हिन्दी पट्टी में आप देखेंगे हिन्दी के साथ कई अन्य स्थानीय बोलियां बोली जाती हैं। ये हिन्दी से पहले भी थी और आज भी हैं। अतः हिन्दी पर इन आंचलिक बोलियों का प्रभाव लाजमी है। चूँकि लोग घरों में जन्म के प्रारंभिक वर्षों में आंचलिक बोलियां ही प्रयोग करते हैं, अतः उनमें स्थानीय भाषाई संस्कार स्वतः विकसित हो जाते हैं। बाद में जब वे हिन्दी भी बोलते हैं तब स्थानीय भाषा के आरोह-अवरोह, शब्द, शैली और लाक्षणिकता भी प्रकट होते हैं। यही कारण है की समान्य बातचित से ही हम व्यक्ति विशेष के जनांकिकी और क्षेत्रीय आधार को आसानी से समझ जाते हैं। अकेले बिहार के जनांकिकीय स्वरूप पर गौर करें तो देखते हैं की यहाँ उत्तर से दक्षिण तक बोलियों में खासी विविधता है। यहाँ हिन्दी के अतिरिक्त भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, अंगिका मगधी या मगही आदि बोली जाती। उसी प्रकार झारखंड में खोरठा, नागपुरिया, पंचपरगनिया का प्रयोग होता है। इनके साथ समानांतर रूप से हिन्दी भी बोली जाती है। अतः प्रारंभिक भाषा संस्कार का प्रभाव अनुगामी हिन्दी पर भी पड़ता है। जैसे संयुक्त बिहार की किसी भी भाषा में लिंग की स्पष्टता पर बल नहीं दिया जाता है,भाषा में” मैं” जैसे सर्वनाम का अभाव है, ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, एक वचन और बहु वचन की स्पष्टता पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप जब हिन्दी में स्थानीय बातचीत करते हैं तब इन क्षेत्रों में गलतियाँ स्वभाविक रूप से होती हैं। जहाँ तक शैक्षणिक परिदृश्य का सवाल है, विद्यालयों में भी विद्यार्थी प्रारंभिक वर्षों में इन विसंगतियों पर ध्यान नहीं देते। घरों में, विद्यालयों या बाजारों में उनके संपर्क की भाषा स्थानीय मिश्रित हिन्दी ही होती है। मानक हिन्दी उन्हे महज पाठ्य पुस्तक में ही मिलती है। मानक हिन्दी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों से संपर्क न के बराबर ही होता है। यहाँ तक कि विद्यालय में शिक्षक भी मानक हिन्दी का प्रयोग नहीं करते हैं, परिणामस्वरूप अशुद्धियां की आदत सी हो जाती हैं। यही हाल पश्चिमी भारत का है, इन क्षेत्रों में भी स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जैसे दही खट्टी है, चीनी मीठी है। हाँ इन क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में भी ने विभक्ति का प्रयोग होने से हिन्दी में स्वतः प्रयुक्त होने लगती हैं। फिर भी ना खड़ी हिन्दी हरियाणा में बोली जाती है न झारखंड में। यह सहारनपुर, मेरठ , बिजनौर, मुरादाबाद आदि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, वह भी शिक्षित तबके तक। अतः इस दिशा में थोड़ी जागरुकता जरूरी है। उस दृष्टि से सबसे अधिक जवाबदेही प्राथमिक शिक्षकों की बनती है। यदि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्वयं खड़ी हिन्दी और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेंगे तो बच्चे स्वतः उनका अनुकरण करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे एक करीबी प्रोफेसर साहब के परिवार में सारे लोग अच्छी हिन्दी बोलते और लिखते थे। यहाँ तक कि उनके नौकर और नौकरानी के उच्चारण और वाक्य रचना शुद्ध हुआ करते थे। मेरे आश्चर्य का उत्तर सिर्फ इतना था कि उनके संपर्क और संस्कार मानक और स्तरीय थे। यदि संपर्क आम लोगों के भी मानक हो जाएं तो उनकी भाषा भी सुधर सकती है। लिखते समय शुद्धता के प्रति हम अतिरिक्त सतर्क होते हैं अतः गलतियाँ कम होती है। फिर भी उच्चारण संबंधी लापरवाही के कारण वर्तनी सबंधी गलतियाँ होती हैं। अतः भाषा संबंधी मानक व्यवहार और संस्कारों की आधारशिला प्राथमिक स्तर पर ही आरोपित होने चाहिए। फिर भी यह हिन्दी है, हमारी अपनी भाषा है। सुनकर अपना सा लगता है। इसमे अनपढ़, ज्ञानी, कुपढ सबका गुजारा हो जाता है। इसमे ही सारी बोलियों, उपभाषाओं, तबकों को समाहित कर आगे बढ़ने की पूरी क्षमता और संभावना है। जरूरत है हम विद्यार्थियों को आगे आने की ताकि भाषाई संस्कारों में सुधार के द्वारा आंचलिक लाक्षणिकता के साथ इसके परिमार्जन और सम्मोहन को सुगम बनाया जा सके। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी हिन्दी के सुधि साधकों को अनेकशः अग्रिम शुभकामनाएं।
पुनश्च,….. जय हिन्दी, विजय हिन्दी, समृद्ध हिन्दी।
जयंत चक्रपाणी, शिक्षक